एक ऐसे संक्रान्ति काल में जब एक ओर ‘जेनरेशन गैप’ की निरंतर चौड़ी होती हुई खाई ‘वर्तमान में जीने के फैशन’ का प्रचलन तथाए ‘मार्केटिंगश् अथवा ‘बिकने-बेचे जाने वाले के कौशल’ का महिमामंडन ही नहीं वह आजीविका का चरम लक्ष्य बन गया हो; ऐसे काल में जहाँ आदमी एक ही साथ कई चेहरे ओढ़ने के लिए बाध्य हो, दफतर-दुकान में अलग, घर-परिवार में अलग, वोट डालते समय अलग, बच्चों को ‘होमवर्क’ कराते समय अलग, टिकट खिड़की पर टिकट खरीदते समय अलग, तो ऐसे समाज से किसी गंभीर चिन्तन की अपेक्षा करना व्यर्थ है। परंतु इन्हीं अतिरेक की स्थितियों में हम आप सभी कुछ क्षण विश्रान्त होना चाहते हैं। जिसमें बहुधा हम गप-शप और अपना मनोरंजन करते हैं। ऐसे में यदि कोई गंभीर बात की जाए तो उसे कौन सुनेगा? परंतु इस स्थिति में भी जब आपने यह पुस्तक उठा ही लिया है और ये लाइनें पढ़ रहे हैं। तो निश्चय ही आप कुछ चुने हुए लोगों में से हैं। और सामान्यतः ऐसे ही कुछ चुने हुए लोगों के लिए यह पुस्तक ‘राष्ट्रीयता दर्शन और अभिव्यक्ति’ है।
देश, राष्ट्र, मानवता और विश्व बन्धुत्व के उदात्त विचारों ने कभी न कभी सभी विचारशील व्यक्तियों को आकर्षित किया है। ‘राष्ट्र’, किसी देश विशेष के लिए प्रयुक्त क्षेत्र का बोधक शब्द नहीं है, हिदुस्तान में यह भाववाचक-संज्ञा भी है, किसी चिन्तन धारा राजनीतिक हिन्दूवाद या किसी अति भावुक उदगार के कारण से नहीं, वरन् उससे भी परे किसी उच्चतर उदगम से निःसृत होने के कारण कोई देश अपने सच्चे निहितार्थ में वास्तविक राष्ट्र होता है।
इस पुस्तक के लेखक एक विशिष्ट व्यक्ति कहे जा सकते हैं। उनकी वृत्ति लेखन नहीं है बल्कि वह आध्यात्मिक साधक हैं। ऐसे साधक जो कुछ कहते हैं तो उसके पीछे उनकी लोक प्रशंसा की आशा और संकुचित स्वार्थ नहीं वरन् साधना की प्रत्यक्ष अनुभूति होती है। यह इसी बात से सिद्ध है कि लेखक कतिपय आध्यात्मिक पत्रिकाओं जैसे श्री अरविन्द कर्मधारा जैसी पत्रिकाओं में अपने आध्यात्मिक अनुभवों को बाँटने की सदिच्छा से ही लिखते रहे हैं। धर्म और दर्शन के गहन अध्येता और एक साधक होने के कारण उन्होंने जो भी स्वान्तः सुखाय या आत्मविश्लेषण स्वरुप लिखा है उसमें से बहुत कुछ अब श्री वह एकान्तिक बनाये हुए हैं। कारण उनमें न तो व्यवासायिक न ही आत्म-प्रदर्शन की इच्छा रही है। यहाँ तक कि जब उन्होंने अपनी एक रचना को जिसे वे ‘संकलन’ कहना पसंद करते हैं, जब अपने कुछ मित्रों को दिखलाया तो किसी ने उसकी एक प्रति उत्तर-प्रदेश सरकार को भेजने के लिए प्रेरित कर दिया और जब शासन ने उन्हें इसके प्रकाशन में आर्थिक सहायता प्रदान की तो वे विचलित हो गये, प्रसन्नता के मारे नहीं, वरन् स्वीकृत धनराशि का ईमानदारी से सदुपयोग करने के लिए और इस क्रम में उन्हें आर्थिक कठिनाइयों से भी जूझना पड़ा। आज उनकी वह रचना ‘एक मन की आध्यात्मिक यात्रा’ अनेक साधकों की मार्गदर्शिका है। ऐसी ही है प्रस्तुत पुस्तक के लेखक की वृति, उनका विलक्षण अध्ययन, साधना और अध्यवसाय।
प्रस्तुत पुस्तक का विषय वस्तु समसामयिक है। प्रथम दृष्ट्रया तो प्रतीत होगा कि लेखक शायद राजनीति अभिप्रेरित राष्ट्र की बात करेंगे परंतु आश्चर्य होता है कि उन्होंने इस शब्द (राष्ट्र) को विक्रमशिला और नालंदा के प्राचीन पुस्तकों की राख, असंख्य भारतीय और योरोपीय दर्शनों के मलबे में से निकाल कर, झाड़-पोंछ कर, वर्तमान युग के संदर्भ में, वैदिक कालीन गरिमा के प्रकाश-स्तंभ के रूप में स्थापित किया है। राष्ट्रीयता की वर्तमान अस्पष्ट एवं संकुचित संकल्पना को प्राचीन भारतीय अवधारणा वैदिक काल के मंतव्य और अभिप्राय की कालजयी ऐतिहासिक यात्रा के परिपेक्ष्य में उन्होंने प्रस्तुत करने का यत्न किया है। ऐसा करते हुए लेखक ने पहले वास्तविक राष्ट्रीयता का स्वरूप स्पष्ट करने का प्रयास किया है। उसकी दार्शनिक, आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक विवेचना की है। ऐसा करने में अनिवार्यतः उन्हें गहन दार्शनिक-प्रत्ययों और राजनीति-शास्त्र के रणांगण से निकलकर, परामनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों में प्रवेश करना पड़ा है। पुस्तक पढ़ते हुए लगता है कि लेखक प्राचीन भारत के विराट भग्नावशेषों से अभिभूत हो उठ है तथा राष्ट्र को वह समष्ठि के एक आदर्श धर्म या रिलिजन के रूप में स्थापित कराना चाहते हैं पर ऐसा है नहीं। लेखक की दृष्टि समष्टि की सामाजिक मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक अवधारणा से भी आगे है। ‘प्रकृतिस्थ-पुरूष की खोज तो सच्ची आध्यात्मिक सत्ता के जागरण का केवल पहला पग होता है’। वह व्यक्ति और समिष्ट में बिना भेद एवं पक्षपात किये कम से कम तीन उच्चतर रूपान्तरणों की बात करते हैं। और तब समझ में आता है कि लेखक ने श्री अरविन्द के योग का एक आध्यात्मिक साधक होने के अपने धर्म और दिव्य चेतना के उच्चतरों से प्रेरित होकर ही इस पुस्तक का सृजन किया है।
कुछ लोगों को लेखक द्वारा महर्षि श्री अरविन्द के ‘पूर्ण-योग’ के दर्शन को बार-बार उदधृत करना खटक सकता है। परंतु क्या किया जाए? लाचारी है, अन्य किसी मनीषी ने तो अतिमन, विकसनशील अध्यात्मिकता, और चैत्य पुरूष की अवधारणा प्रस्तुत करते हुए वर्तमान यथार्थ की निम्नतर चेतना-स्तर की कंक्रीट की नींव ( तारकोल, खेत, खलिहानों के जगत और हाड़-मांस के मनुष्यद्) और ‘सर्वोच्च अध्यात्मिक चेतना स्तर’ के बीच ‘लिंक’ (सेतु) बनाने और जड़ भौतिक में तदनुसार उस आध्याम्तिक चेतना की अभिव्यक्ति का प्रयास और उसकी सफलता का आश्वासन भी तो नहीं दिया। मेरी समझ में पुस्तक की समस्त गरिमा ‘अनिर्वचनीय’ को ‘वर्चनीय’ ‘अमूर्त’ को ‘मूर्त’ करने का उपाय बताने में निहित है।
अन्त में, मैं यह स्वीकार करना चाहूँगा कि मैं अपने को पुस्तक के विषय-वस्तु पर कुछ कहने का अधिकारी विद्वान नहीं समझता परंतु, लेखक के आग्रह पर अपने दो शब्द कहने से मैं अपने को रोक भी नहीं पा रहा हूँ। अस्तु, भारी मन से मैं यह धृष्टता कर रहा हूँ। इस प्रकार की धृष्टताओं के औचित्य के संबध में विश्वविद्यालय-शिक्षा से वंचित मनीषी, महापंडित राहुल सांकृत्यान के शब्दों को उद्धरित करता हूँ-“ऐसी धृष्टता के लिए मैं मजबूर था। जब तक अधिकारी व्यक्ति हिन्दी तथा केवल हिन्दी-दाँ जनता को अपनी कृपा का पात्र नहीं समझते तब तक मेरे जैसे अनधिकारियों को धृष्टता करनी ही होगी।“ (“विश्व की रूपरेखा”, प्र॰सं॰-1944 ‘प्रक्कथन’ से)।
सतीशचन्द्र श्रीवास्तव ‘सफरचंद’
668/8 रामेश्वरपुरी, बस्ती (उ॰प्र॰)
skip to main |
skip to sidebar

Thursday, January 21, 2010
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
पुस्तकालय
-
▼
2010
(8)
-
▼
January
(8)
- इतिहास- प्राचीन इतिहासः डॉ॰ आर के शुक्ला
- इतिहास व संस्कृति- कहलूर-बिलासपुरः डॉ॰ आर के शुक्ला
- कविता संग्रह- साया- रंजना भाटिया 'रंजू'
- कविता-संग्रहः अनुभूतियाँ- दीपक चौरसिया 'मशाल'
- कविता संग्रह- शोर के पड़ोस में चुप सी नदी- मनीष मिश्र
- जीवनी- भगत सिंहः इतिहास के कुछ और पन्ने- प्रेमचंद ...
- कविता संग्रह- पतझड़ सावन वसंत बहार- अनुराग शर्मा
- निबंध संग्रह - राष्ट्रीयता दर्शन और अभिव्यक्ति - अ...
-
▼
January
(8)



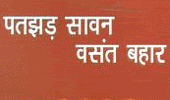
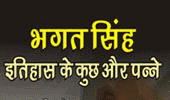




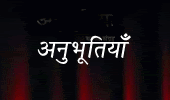


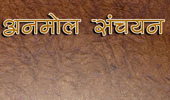

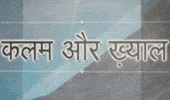

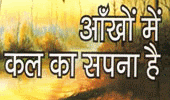
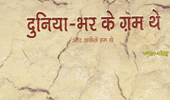
आप क्या कहना चाहेंगे? (post your comment)
3 पुस्तकप्रेमियों का कहना है कि :
useless site
boring and time wastage
बेहतरीन जानकारी है। आभार।
आप क्या कहना चाहेंगे? (post your comment)